व्यक्तिगत, व्यवसायिक और सामाजिक जीवन में सामंजस्य
अति सर्वत्र वर्जयेत्

ब्रह्मांड के संचालन से लेकर मानव शरीर के निर्माण व जीवन निर्वह्न में सामंजस्य का बहुत महत्व है। व्यक्ति के जीवन निर्वहन की प्रकृति उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जन्म देती है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने ज्ञान और कौशल के अनुरूप व्यवसाय करता है, व्यवसाय उसे समाज से जुड़ने का अवसर देता है। एक ही व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत, व्यवसायिक और सामाजिक क्रियाकलापों को करता है इसलिए इनके बीच भी सामंजस्य होना अति आवश्यक है। सामंजस्य के अभाव में व्यक्ति तनाव से ग्रस्त होता है जो उसके जीवन में उमंग को दुष्प्रभावित करता है।
:प्रेम कुमार । kumarprem.in
परिचय

मनुष्य ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, सृष्टि अथवा ब्रह्मांड को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है जिसमें सूर्य, अन्य तारे, ग्रह, उपग्रह, शुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड इत्यादि हैं। ये सभी सुर में सुर मिला कर संतुलन के नियम का पालन करते हुए, अपनी धुरी पर चिरकाल से संचालित होते आ रहे हैं। इनमें से धरती में जीवन को संभव करने के लिए समस्त प्राकृतिक तत्व और सम्पदाएं संतुलित मात्रा में उपलब्ध है, जैसे जल, वायु, स्थल, अग्नि व आकाश इत्यादि। इन तत्वों के असंतुलित होने मात्र से ही सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इस धरती में मानव मात्र के शरीर को देखा जाए तो इसकी संरचना में भी संतुलन का बहुत बड़ा भूमिका है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर के तीन घटक वात, पित्त और कफ के असंतुलित होने से ही इसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं।
श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं:
क्षिति गगन जल पावक समीरा।
पांच तत्व मिली अधम शरीरा॥अर्थात धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु इन पांच तत्व के संतुलित मिश्रण से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है।
:तुलसी दास
ब्रह्मांड के संचालन से लेकर मानव शरीर के निर्माण व जीवन निर्वह्न में संतुलन का बहुत महत्व है। किसी मानव या व्यक्ति के जीवन निर्वहन की प्रकृति अथवा तौर तरीका उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जन्म देती है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने ज्ञान और हुनर के अनुरूप व्यवसाय का चयन करता है, व्यवसाय उसे एक तरीके से समाज से जुड़ने का अवसर देता है। एक ही व्यक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक क्रियाकलापों को करता है, इसलिए इनके बीच भी संतुलन होना अति आवश्यक है। इनके बीच संतुलन के अभाव में व्यक्ति तनाव से ग्रस्थ होता है जो जीवन में खुशी और उमंग को दुष्प्रभावित करता है। जीवन में आनंद नहीं होने से जीवन व्यर्थ और कष्टदायी प्रतित होता है और व्यक्ति मज़बुरियों के बीच फस कर जीवन को बोझ समझ कर जीता है।
व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन का रचना
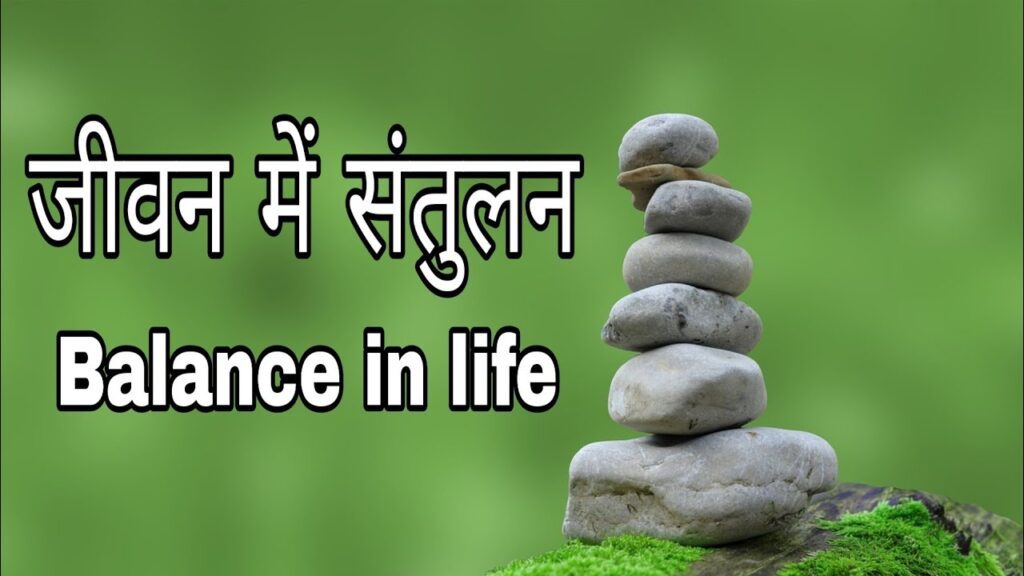
व्यक्तिगत जीवन
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस धरती पर अकेला निवास नहीं कर सकता, इसलिए मनुष्य परिवार, रिश्तेदार, व्यवसाय और समाज का निर्माण करता है जो उसके जीवन को विभिन्न तरीकों से सार्थक, सुलभ और आसान बनाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का परिवेश मुख्य रूप से व्यक्ति के परिवार, रिश्तेदार और निजी क्रियाकलापों से बनता है। व्यक्ति अपने परिवेश में निर्वहन करते हुए अपनी आवश्यकताओं को जन्म देता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं में केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं होता है अपितु व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी परिवार में विभिन्न रिश्तों के बंधन से बंधा होता है इसलिए अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं भविष्य की संभावनाओं से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं का भी ख्याल रखता है।
व्यावसायिक जीवन
व्यक्तिगत जीवन का परिवेश जिन आवश्यकताओं को जन्म देता है उसकी पूर्ति के लिए वर्तमान समय में धन उपार्जन करना अति आवश्यक हो जाता है। धन के अभाव में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता इसलिए धन उपार्जन करने के लिए व्यक्ति अपने कौशल और ज्ञान के अनुरूप व्यवसाय, नियोजन, रोजगार, स्वरोजगार आदि आर्थिक गतिविधियों का चयन करता है। कुल मिला कर इस लेख में हम आर्थिक क्रियाकलापों से धन उपार्जन की व्यवस्था को व्यवसाय कहेंगे। व्यवसाय वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से धन उपार्जन के लिए एक व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करता है या विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है।
सामाजिक जीवन
कोई व्यवसाय बड़ा, छोटा, नया, पुराना, पैतृक अथवा आरम्भिक हो सकता है किंतु किसी भी व्यवसाय में धन उपार्जन के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री होना आवश्यक है। वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के लिए ग्राहक का होना आवश्यक है। किसी व्यवसाय में उपलब्ध वस्तु अथवा सेवाओं के आधार पर ग्राहक भी होते हैं। ग्राहक किसी भी क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, जाति अथवा धर्म का हो सकता है। इसलिए व्यवसाय हमें विभिन्न प्रकार के समाज से जुड़े लोगों से समन्वय स्थापित करने का अवसर देता है या यूं कहें तो व्यवसाय एक तरीके से हमें समाज से जुड़ने का मौका देता है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ने के साथ – साथ प्रतिस्पर्धा के इस दौर में व्यावसायिक जीवन में व्यक्ति अपने ग्राहकों से कुशल व्यवहार के साथ व्यावसायिक समन्वय स्थापित करने के लिए जुड़ता है जिससे धन उपार्जन हो।
जैसा कि हमने देखा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति व्यवसाय का चयन करता है और व्यवसाय में धन उपार्जन के लिए व्यक्ति समाज से समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार से समाज का हमारे जीवन में व्यापक प्रभाव पड़ता है। वैसे समाज का केवल यही स्वरूप नहीं है। समाज बहुत ही विशाल और विस्तृत पहलू है जिसे संक्षेप में समझ पाना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम, ज्ञान, कार्य, व्यवसाय, प्रतिभा, कद काठी के सम्मिलित रूप में अपना एक अद्वितीय पहचान रखता है लेकिन कई रूपों में व्यक्ति का क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, समस्या, लक्ष्य, प्राथमिकता अथवा कार्य आदि दुसरे व्यक्तियों के समान होता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के समान हैं, उस रूप में वे एक समुदाय का निर्माण करता है और समुदाय के संगठित रूप को ही समाज कहा जाता है।
दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो एक व्यक्ति अपने दिनचर्या में प्रयोग होने वाले सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का स्वत: ही निर्माण कर उनका प्रयोग नहीं कर सकता। उदाहरण स्वरूप हमारे रसोई में बनने वाले भोजन में उपयोग होने वाले प्रत्येक घटक जैसे दाल, चावल, चना, तेल, सब्जी, मसाले, नमक आदि का उत्पादन खुद ही करें फिर भोजन बनाएं, हम जो वस्त्र पहनते हैं उस वस्त्र में प्रयोग होने वाला धागा से लेकर कपड़ा खुद ही तैयार करें खुद ही सिलाई करें फिर पहने या हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान में प्रयोग होने वाले ईट, सीमेंट, बालू, रॉड आदि का निर्माण खुद ही करें एवं खुद ही मजदूर तथा कारीगर बनकर घर का निर्माण करें। ऐसा कर पाना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है इसलिए हम अपनी जीवन को सुखद, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हुनरवान सहयोगियों अथवा व्यवसायियों की सहायता लेते हैं। जैसे किसान हमारे लिए अनाज उगाता है, मजदूर घर बनाते हैं अथवा अन्य पारिश्रमिक कार्य करते हैं, मोची जूता सिलता है, दर्जी कपड़े सिलता है इत्यादि प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुरूप हमारी मदद करता है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति इस बात को भली-भांति एहसास करता है और अपनी समाज से पुरी होने वाली आवश्यकताओं के मद्दे नज़र समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है।
व्यक्ति किसी न किसी रूप से किसी समुदाय से ताल्लुक रखता है एवं उसे दूसरे समुदाय अथवा व्यक्ति की सहायता अपनी दिनचर्या के कार्यों का निपटारा करने के लिए लेनी ही पडती है, भले ही उसे इस कार्य के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़े। ये सभी समुदाय अथवा व्यक्ति विशेष समाज के घटक हैं और संगठित रूप में समाज का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन में हम अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, व्यावसायिक जीवन में हम अपने ग्राहकों अथवा उपभोक्ताओं से व्यावसायिक समन्वय स्थापित करने के लिए जुड़ते हैं उसी प्रकार सामाजिक जीवन में हम समाज के विभिन्न घटकों के प्रति अपने व्यवहार में विनम्रता और आदर का भाव रखना चाहिए इससे अपने आप और समाज के बीच संतुलन बनाना आसान होता है।
व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तिगत, व्यावसायिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों को करता है जिसके कारण उसकी दिनचर्या तीन रूपों में बट जाती है, इसमें संतुलन के लिए व्यक्तिगत जीवन में भावनाओं का ज्यादा महत्व होता है, व्यावसायिक जीवन में कुशल व्यवहार व समन्वय का ज्यादा महत्व होता है एवं सामाजिक जीवन में एक दूसरे के प्रति आदर का ज्यादा महत्व होता है।
अति का दुष्प्रभाव

व्यक्तिगत जीवन में
किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक संलिप्तता होने से ही हमारा जीवन असंतुलित होता है उदाहरण स्वरूप देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति और विलासिता के लिए ही केवल लीन रहता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। वह व्यवसाय और समाज से उतना ही ताल्लुक रखता है जितने में उसकी विलासिता पूर्ण हो। लेकिन विचार किया जाए तो विलासिता हमें भौतिक सुख प्रदान कर सकता है किंतु आनंद नहीं दे सकता। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति के प्रति लोगों की कृतज्ञता व विश्वसनीयता कम या खत्म हो जाती है और ऐसे व्यक्ति से लोग भी स्वार्थपूर्ण ही संबंध रखते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी आनंदित जीवन नहीं जी सकते हैं।
इस विषय में कबीर जी का कथन है:
:कबीर
मैं-मैं बड़ी बलाई है, सकै तो निकसो भागी।
कब लग राखि हे सखी, रूई लिपटे आगी॥
अर्थात् केवल मेरा ही भला हो, ऐसा स्वार्थपूर्ण सोच बहुत ही बड़ी विपदा है, जितना जल्दी संभव हो ऐसे सोच का त्याग कर देना चाहिए। अपने मन मस्तिष्क में ऐसा स्वार्थपूर्ण विचार रखना, रूई में आग को लपेटकर रखने के समान है। आग अंततः हुई को जला ही देगी।
व्यावसायिक जीवन में
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति धन के सार्थक प्रयोग को जाने बिना अपने व्यावसायिक जीवन में धन उपार्जन के लिए ही केवल लीन रहता है तो ऐसा व्यक्ति कोल्हू के बैल के जैसा होता है जो केवल तेल निकालने के लिए ही जानता है भले ही उस तेल का प्रयोग उसके भोजन अथवा उसके मालिश के लिए ना किया जाए। धन के सार्थक प्रयोग को जाने बिना व्यक्ति अगर आवश्यकता से अधिक धन उपार्जन कर भी ले तो वह उसके लिए कभी सार्थक नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए इंधन की सार्थक उपलब्धता उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उसके ईंधन की टंकी की क्षमता है। यदि उस मोटरसाइकिल के आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह ईंधन का गेलन बांध दिया जाए तो इस मोटरसाइकिल को बर्बाद होने के लिए केवल एक माचिस की तिल्ली अथवा एक छोटी सी दुर्घटना में एक चिंगारी ही काफी होगी। उसी प्रकार हमारे जीवन में धन की आवश्यकता उतनी ही है जितनी हम उसका सार्थक उपयोग कर सकें, उससे अधिक होने पर हमारे जीवन में भी आग लग सकती है।
इस विषय में कबीर जी कहते हैं:
:कबीर दास
कबीरा सो धन संचे, जो आगे को होय।
सीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देख्यो कोय॥
अर्थात हमें केवल रुपया पैसा नहीं बल्कि ऐसे धन का संचय करना चाहिए जो हमें भविष्य में हर एक परिस्थिति में काम आवे। मरने के बाद सर पर धन की पोटली लेकर जाते हुए किसी को नहीं देखा गया है।
सामाजिक जीवन में
कोई व्यक्ति सामाजिक जीवन में अत्यधिक संलिप्तता रहे तो उसका व्यक्तिगत जीवन समयाभाव के कारण कल्ह का घर बन जाता है। व्यवसाय भी ठीक-ठाक तरीके से नहीं चलने के कारण धन का अभाव रहता है। हमने जितना अनुभव किया है उससे यही पता चलता है कि ईमानदारी से केवल समाज सेवा करने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन बहुत ही दयनीय होता है। उसके घर में व्यक्तिगत समस्याएं और धन का अभाव हमेशा हावी रहता है। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह केवल समाज सेवा ही करता है, धन उपार्जन के लिए उसका कोई व्यवसाय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति समाज सेवा से ही धन उपार्जन का रास्ता ढूंढने का प्रयास करता है या फिर समाज सेवा को ही धन उपार्जन का माध्यम बना लेता है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति ना ईमानदारी से समाज सेवा करने का दावा कर सकता है ना ही समाज सेवा को अपने व्यवसाय के रूप में घोषित कर सकता है।
यदि हम हमारी गगरी भरने के बाद बचने वाले अतिरिक्त जल का प्रयोग लोगों की प्यास बुझाने में करते हैं तो यह बहुत ही सार्थक कार्य होता है। ऐसी अवस्था में हम खुद भी सुखी रहता है और क्षमता के अनुसार औरों को भी खुश करने का प्रयास करता है, लोग भी हमसे प्रसन्न रहते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपनी गगरी में जितना भी जल बचा है उसका प्रयोग लोगों की प्यास बुझाने में करता है तो गगरी खाली होने के बाद ना वह खुद की प्यास बुझा सकता है और ना ही लोगों की प्यास बुझा सकता है। ऐसी अवस्था में भी लोग उससे वैसा ही उम्मीद रखते हैं जैसा वह पहले रखा करते थे। यदि लोगों का उम्मीद टूटता है तो व्यक्ति उनकी नजरों में गिर जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपकी गगरी झांक कर नहीं देखता कि पानी है या नहीं। अधिकतर अवस्था में उसे केवल अपनी प्यास बुझाने से मतलब होता है।
इसलिए इमानदारी से समाज सेवा करने के लिए हमारे पास एक सुदृढ़ व्यवसाय होना चाहिए जिससे हम आजिवीकोपार्जन करके अपना घर चला सके। एक बीमार डॉक्टर ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकता, उसे पहले अपनी बीमारी ठीक कर लेनी चाहिए।
इस विषय में कबीर जी कहते हैं:
:कबीर दास
साईं इतना दीजिये, जा मे कुटुम समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ, साधु ना भूखा जाय॥
जीवन में संतुलन, उसका महत्व और तरीका
व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवन के विवरण में हमने देखा कि किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक संलिप्त रहने का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। अब सवाल उत्पन्न होता है कि व्यक्तिगत, व्यावसायिक अथवा सामाजिक जीवन में संतुलन बनाने का महत्व और तरीका क्या है?

महत्व
व्यक्तिगत, व्यावसायिक तथा सामाजिक जीवन में संतुलन बनाने का बड़ा ही महत्व है। हम तनाव मुक्त जीवन जीते हैं। हमारे सभी कार्य सही समय पर पूर्ण होते हैं और जीवन अधूरे कार्यों से भरा हुआ प्रतीत नहीं होता है। हमारा जीवन आनंद से भरपूर होता है जिसके कारण हममें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमें हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण लगता है। संतुलित अवस्था में हम जीवन को जी रहे होते हैं ना कि किसी तरह बस काट रहे हैं। लोग हमसे जुड़ना पसंद करते हैं और हम सभी के लिए खुशी की वजह बनते हैं। संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा कल के चुनौतियों के लिए तैयार रहता है।
तरीका
व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बनाने का तरीका यही है कि
- हम आज के कार्यों को बेवजह कल पर ना टालें।
- ऑफिस के कार्यों को घर पर और घर के कार्यों को ऑफिस पर या व्यवसाय में ना करें।
- अपने व्यक्तिगत कार्यों को सम्भवतः खुद ही करें, हर वक्त दुसरों पर आश्रित ना रहें।
- एक वक्त में करने के लिए केवल एक ही कार्य का आबंटन करें।
- एक ही समय पर व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन के कार्यों को करने की परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उनके बीच प्राथमिकता तय करें।
- आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन एक ही वक्त पर नहीं इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य का चयन सर्वप्रथम करें।
- ज्यादा व्यस्तता की स्थिति में अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए अपने सहयोगियों, कर्मचारियों और रिश्तेदारों को योग्यता अनुरूप कार्यों का आबंटन करें।
- नियमित अंतराल में अपने लिए वक्त निकालें।
- अपने स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था और धन का ख्याल रखें, बेवजह या गौण कार्यों में व्यर्थ ना करें।
ऐसे ही आवश्यकता अनुरूप अन्य बातों का ध्यान रख कर हम अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं।
निष्कर्श:
निष्कर्ष यही निकलता है कि जीवन के निर्वहन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक कार्यों को करना पड़ता है फिर भी इनके बीच संतुलन होना अति आवश्यक है। ऐसा कर पाना प्रारंभ में मुश्किल कार्य प्रतीत हो सकता है लेकिन समय उपरांत हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, सार्थक, आनंदित और मनोरंजन से भरा महसूस करते हैं। किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक संलिप्तता हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है हमारे वेदों में भी कहा गया है: अति सर्वत्र वर्जयेत् अर्थात् किसी भी कार्य में अत्यधिक संलिप्तता से हमें बचना चाहिए। अपने आवश्यकता अनुरूप जीवन को संतुलित करने के तरीकों का प्रयोग करके हम अपना जीवन संतुलित कर सकता है।
धन्यवाद !
